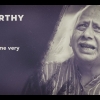चित्र: महेंद्र साव, सलहेस लोक-कलाकार, बेतौनहा, मधुबनी, 2016 । फोटोग्राफर - सुनील कुमार
मधुबनी के घोघरडीहा में देर रात तक चल रहे एक लोकनाट्य का दृश्य, मंच पर गर्व से लबरेज नायक के कई संवादों में से कुछ की बानगी:-
नायक का अपना परिचयात्मक संवाद -
हमरो जे घर यौ पंचन
राज छै महिसौथा मे।
हमरो जे नान यौ पंचन
राजा सलहेस छै।
मझिला के ना छै मालिक
मोतीराम दुलरूआ ने हो
छोटकाके नाम मालिक
बौआ बुधेसर लगै छै।
संवाद दो - बल से लड़तै बल से लड़बै / छल से लड़तै छल से लड़बै
संवाद तीन – अस्सी मनक डंटा उटौलकै / जहिना बान्ह सहोदराक बन्हली / तहिना भेंट हां राजा क देवै / बाप से भेंट आइ तोरा करा देबौ
संवाद चार – बाप से तS भेंट करबेह राज तS बरांटपुर में आ बाप से तS भेंट करेबह राज तS बरांटपुर में और इस तरह नाटक आगे बढ़ता है।
लोकनाट्य राजा सलहेस के संवादों को पढ़कर यह महसूस नहीं होता है कि अलग-अलग विशेषताएं लिये ये संवाद लोकगाथाओं के विस्मरण के इस काल में भी कितने लोकप्रिय हैं। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस समय मंच पर ये संवाद पूरी शिद्दत के साथ एक अभिनेता अदा कर रहा था, उसी समय मंच के नीचे और अभिनेता से कम शिद्दत के साथ नहीं, बल्कि कई जगहों पर उससे भी ज्यादा शिद्दत के साथ उसके प्रेक्षक भी संवाद की अदायगी कर रहे थे।
लोकगाथा राजा सलहेस पर विस्तार से चर्चा से पूर्व कुछ प्रसंगों पर नजर डालिये। (प्रसंग एक) पकड़ियागढ़ का राजा कुलेश्वर सोंटा सिंह (दोनों नाटक के किरदार) से कहता है कि सलहेस को जेल में बंद कर दो और उसकी छाती पर अस्सी मन का खंडा रख दो, तब सोंटा सिंह जवाब देता है कि अस्सी मन का खंडा क्यों रखें, इसे जनकपुर के हॉस्पिटल में छोड़ दिया जाये, मच्छर और मक्खियां इसे मारकर खा जाएंगी।
संवाद एक- जातीय परिचय, संवाद दो- कूटनीतिक परिचय, संवाद तीन व चार- बाहुलबल यानी शक्तिबल परिचय और उपरोक्त संवाद यानी समसमायिकता से परिचय, यह लोकगाथा राजा सलहेस की अनेक चारित्रगत विशेषताओं में कुछेक हैं जो मौजूदा समाज और उसकी सामाजिक व्यवस्थाओं को प्रतिबिंबित करती हैं। यह प्रतिबिंबन समाज की संपूर्ण सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास की थाती को भी आत्मसात करते चले जाने के कारण संभव होता है। रंग-कला विधानों में, जिसमें पूजा-पाठ, तीज-त्योहार आदि शामिल हैं, उनकी गीतीमय प्रस्तुतियों के जरिए जनसामान्य के समक्ष उनकी अभिव्यक्ति होती है। इस लिहाज से लोकगाथा राजा सलहेस उन कुछेक लोकगाथाओं में से एक है जो लोक अभिव्यक्ति के सभी माध्यमों में प्रमुखता से अभिव्यक्त होती हैं। चाहे वह लोकरंग कर्म हो, लोकगीत हों, या फिर लोक-चित्रकला या मूर्तिकला। इस लिहाज से अगर यह कहा जाए कि लोकगाथा राजा सलहेस ने बिहार में अपनी ही एक अलग संस्कृति, सलहेस संस्कृति को जन्म दिया है, तो यह गलत नहीं होगा। इस संस्कृति की प्रधानता मिथिलांचल में प्रमुखता से दिखती है और मिथिलांचल के साहित्यकारों और मनीषियों ने राजा सलहेस के इतिहास के साथ-साथ, उसके गीतों, नाटकों और गाथा-कथाओं का एक लंबा इतिहास भी खोज निकाला है, जिसका विस्तार नेपाल तक है।
जहां तक चित्रकला का सवाल है, मिथिलांचल में राजा सलहेस की लोकगाथा पर आधारित चित्रकला की पहचान बहुत पुरानी नहीं है, हांलाकि इस बारे में कोई ठोस खोज अब तक नहीं हुई है। इस बारे में जो भी जानकारियां सामने आयी हैं वह 70 के दशक के आसपास की हैं और उनमें सलहेस का चित्रण महज अलंकारिक था। सत्तर के दशक में महाराष्ट्र व दक्षिण भारत के दलित आंदोलनों का प्रभाव बिहार पहुंचता है और उसका असर बिहार की राजनीतिक पर दिखता है। लगभग इसी काल में दलित चेतना व चिंतन की सुगबुगाहट मिथिलांचल में होती है और 80-90 के दशक में परवान चढती दलित राजनीति में वर्गीय चेतना एवं चिंतन की तीक्ष्णता आती है। चित्रकला से इतर लोकगाथाओं की प्रस्तुतियों और लोकनाटकों में उनकी आवाज कब से मुखर हुई, उसका ठीक-ठीक अनुमान लगा पाना असंभव है। हांलाकि, सलहेस लोकगाथा के संबंध में पहला महत्वपूर्ण कार्य जार्ज ए. ग्रियर्सन ने किया। उन्होंने भारत में भाषाई अध्ययन के दौरान एक डोम गाथा-गायक से राजा सलहेस की लोकगाथा सुनी और एक दस्तावेज के रूप में 1881 में पहली बार उसका मुद्रित स्वरूप अपनी पुस्तक ‘मैथिली क्रेस्टोमैथी एण्ड वॉकेबुलरी’ में सामने रखा। चित्रकला में यही काम किया विलियम जी. आर्चर ने, जिन्होंने 1934 में आए भूकंप के बाद मिथिला के गांवों की ध्वंसित दीवारों पर बने चित्रों को देखा, उनकी फोटोग्राफी की और बाद में एक बड़े फलक पर उसे उजागर किया। लेकिन, यहां महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि वो तस्वीरें ब्राह्मणों और कायस्थों के घरों की दीवारों पर बने चित्रों की थीं, उनमें दलितों के घरों में बने चित्र नहीं मिलते हैं।
आश्चर्य की बात यह है कि मिथिलांचल की कला-संस्कृति में लोकनाट्यों, लोकगाथाओं और चित्रकला पर कई शोध हुए, लेकिन उनमें दलित अभिव्यक्तियों पर सबसे कम ध्यान दिया गया। इसकी एक वजह तो यह है कि ज्यादातर शोधकर्ता समाज के उच्च तबके से थे जिन्हें निचली जातियों और उनके साहित्य में कोई विशेष रूची नहीं थी। इसकी दूसरी वजह ये रही कि ये लोकगाथाएं दबे कुचले लोगों की महत्वकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं जो नवीन प्रतीकों को गढ़ने पर जोर देती हैं। इसे उन्होंने अपने हितों पर आघात समझा और विभिन्न उपायों से उसकी धार कुंद करने की कोशिश की। यह अभिव्यक्ति तब भी परवान चढ़ती जब स्वयं दलित अध्येता उसकी राजनीतिक-सामाजिक व्याखाएं करते और उसके जरिये समाज को जागृत करने का प्रयास करते, लेकिन वो बहुदा अगड़ी जातियों की कल्चरल हेजिमनी का शिकार हो गये। उन्होंने लोकगाथाओं की मूल अभिव्यक्तियों के खिलाफ उन प्रवृतियों को सहजता से स्वीकार कर लिया जो साधन संपन्न समाज द्वारा उन्हीं के शोषण हेतु बनाए गये थे। इन सबने मिलकर लोककलाकारों की स्थिति जर्जर कर दी और वो धीरे-धीरे न केवल हाशिये पर चले गये बल्कि आज विलुप्ती की कगार पर हैं। आज उन लोकगाथाओं की थाती संभालने वाले लोककलाकारों की संख्या ऊंगलियों पर रह गयी है।
मिथिलांचल में लोककला की लंबी परंपरा है, चाहे यह चित्रकला हो, लोकगीत हो, लोकगाथा हो या लोकनाट्य। चूंकि लोक कलाओं की परंपरा समाज से शोषित और वंचितों की परंपरा मानी जाती है, इस समाज ने अपने मनोरंजन और समाजार्थिक हितों की सुरक्षा के लिए अभिव्यक्ति का अपना माध्यम खोजा और उसे अपनाया, जो मौखिक अभिव्यक्तियां थीं। उन्हीं अभिव्यक्तों ने शनै:-शनै: लोकगाथाओं का स्वरूप ले लिया और जो कला के विविध रूपों में प्रकट हुईं, चाहे वो नाच परंपरा हो, गायन परंपरा हो या चित्रकला और मूर्तिकला। इनमें चित्रकला और मूर्तिकला को छोड़कर अन्य सभी विधाओं में कलाकारों की संख्या तेजी से सिमट रही है क्योंकि यह लोक-कर्म उनकी आजीविका चला पाने में अक्षम साबित हो रहा है और उन्हें आजीविका कमाने हेतु रोज नये संघर्षों से जूझना पड़ रहा है। आजीविका के अभाव में सलहेस गाथागायकों व नाच पार्टियों की टीमें न केवल विखंडित हो गयी हैं, बल्कि लोक-संस्कृति की थाति संभाले ये लोक कलाकार अपनी आजीविका कमाने हेतु पंजाब-हरियाणा में खेतों में खाक छान रहे हैं।
चित्रकला और मूर्तिकला के कलाकारों के सामने आजीविका की समस्या उतनी नहीं है लेकिन वो भी अपने पहचान की एक अलग तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। बिहार में लोकगाथा राजा सलहेस के गायन-मंचन से जुड़े कलाकारों की उपरोक्त दुर्दशा के कई कारण मुझे अपने शोध के दौरान समझ में आये। इसमें सबसे प्रमुख है उचित प्रोत्साहन के अभाव में लोककलाकारों का विदूषक बन जाना। सलहेस लोकगाथा गायिकी और नाच का विस्तार 1970 के दशक तक दुसाधों और पासवान समाज के दायरे तक ही मिलता है। 70 और 80 के दशक में जब बिहार में जातीय राजनीति गरमाती है, तब ये कलात्मक अभिव्यक्तियां अपने समाज के गर्भ से बाहर निकलकर सर्वजातीय समाज के बीच आती हैं। मधुबनी के लोककलाकार कुछ हद तक उसका श्रेय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को देते हैं। लेकिन, वो एक और क्रूर सत्य बयान करते हैं कि 90 के दशक में जब लालू प्रसाद सत्तारूढ़ होते हैं तब उनकी कलात्मक अभिव्यक्तियों की धार कुंद होती हैं और लोककलाकार की स्थिति एक विदूषक की हो जाती है। इससे लोककलाकारों में हीन भावना भरी। यह भाव इतना गहरा था कि मधुबनी के दो प्रमुख गाथागायकों बिसुनदेव पासवान और गंगाराम ने अपने परिवार में किसी को लोकगाथा गायन की परंपरा में शामिल नहीं किया। गंगाराम ने अपने तीन बेटे और तीन बेटियों में सिर्फ अपनी एक बेटी को थोड़ा बहुत सलहेस गायन सिखाया। 2016 में एक संक्षिप्त मुलाकात में उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी को थोड़ी बहुत जानकारी दी क्योंकि उसके समक्ष आजीविका का सवाल महत्वपूर्ण नहीं होगा बल्कि शादी ब्याह के बाद इससे उसके परिवार को थोड़ी आर्थिक मदद मिल जाएगी।
यह दुखद है कि गंगाराम 11 नवंबर 2017 को महज 63-64 वर्ष की आयु में गुजर गये। गंगाराम की अपनी नाच मंडली एक दशक पूर्व ही विखंडित हो गयी थी। तीन वर्ष पूर्व घोघरडीहा सलहेस नाच मंडली के संचालक बिसुनदेव पासवान की मंडली भी भंग हो गयी है। बिसुनदेव पासवान अब दलनायक की भूमिका निभाते हैं। सलहेस गाथा गायिकी और नाच को लेकर अपना दर्द बयान करते हुए बिसुनदेव कहते हैं कि उनके आसपास के कई गांवों यथा- जमैला, चपराम, छजना मझौरा, निर्मली, पकड़िया में कभी राजा सलहेस नाच पार्टी हुआ करती थी, अब नहीं हैं। जो कलाकार बचे हैं, उनमें भी अब किसी में अपनी कला परंपरा को जीवित रखने की रूचि नहीं है।
चिकना गांव के ही एक स्थानीय कलाकार राम उदगार पासवान कहते हैं कि पटना में इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे उनके बेटे और यहां तक कि उनकी पत्नी को उनका गायन-वादन या पूजा-मंडलियों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि समाज में उनकी इज्जत नहीं है। उनके बेटे ने साफ-साफ कहा कि इस विधा में इतना पैसा नहीं है कि उससे घर का खर्च चल सके। चपराम में मुख्य रूप से आल्हा उदल का मंचन करने वाले कलाकारों में से एक हरि नारायण कहते हैं कि उचित प्रोत्साहन के अभाव में स्थानीय कलाकारों की आर्थिक स्थिति जर्जर है। ज्यादातर कलाकार या तो दिहाड़ी पर मजदूरी करते हैं या खेतिहर मजदूर है। ऐसे में वो दूसरे प्रदेशों में काम करना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वहां उन्हें उनके श्रम का पारितोषिक ज्यादा मिलता है। हरिनारयण यह भी कहते हैं कि राजा सलहेस के गायन-वादन या मंचन से लोककलाकार इस वजह से भी विमुख हो रहे हैं क्योंकि उन्हें नचनिया, बजनिया, बाइजी, लौंडा, लफुआ या बोंगा कहकर बुलाया जाता है। इससे उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है।
मौसमी बेरोजगारी भी इन कलाकारों की बड़ी समस्या है जिसने नाच और गाथा गायन, वादन की परंपरा का निर्वाह कर रहे कलाकारों को उनकी विधाओं से विमुख किया। नेपाल से सटे उत्तर मधुबनी के जयनगर से लेकर दरभंगा और समस्तीपुर तक ऐसे कलाकार बिखरे हुए हैं जिनके पास न तो आय का कोई साधन है और न ही अपनी खेती। वो या तो मजदूर हैं या खेतिहर मजदूर। यह भी आवश्यक नहीं कि उन्हें लगातार काम मिलता रहे। इसका सीधा असर उनकी कला परंपरा पर पड़ रहा है। कलाकारों की मानें तो जन्माष्टमी से लेकर बसंत पंचमी तक, यानी सितंबर से लेकर जनवरी तक उन्हें अपनी कला को प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। अर्थात् जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, छठ पूजा से लेकर बसंत पंचमी या सरस्वती पूजा तक। लेकिन वीडियो और डीजे का बढ़ता चलन यह अवसर भी उनसे छीन रहा है। त्योहारों के समय के अलावा अक्सर आर्थिक रूप से साधन संपन्न लोग उन्हें अपनी कला के प्रदर्शन का अवसर देते थे, लेकिन यह प्रवृत्ति भी अब खत्म हो चुकी है।
लोककलाकारों के मुताबिक सलहेस गाथा गायन या नाच अक्सर साटा पर आधारित होता है। साटा वह स्थिति है जिसमें आयोजनकर्ता या जजमान कलाकारों को एक निश्चित अवधि में नाच को पूरा करने के लिए अनुबंधित करता है और बदले में एक निश्चित राशि पारितोषिक के रूप में देता है। गाथा गायन या नाच को पूर्ण करने में लगभग सात दिन लगते हैं और कलाकारों को अमूमन 500 रुपये रोज दिया जाता है जिसमें उसके मंचन हेतु आवश्यक वस्तुओं का खर्च भी शामिल होता है। साल में अगर ऐसे चार पांच साटा लग भी जाये तो कलाकारों की माली हालत अंदाजा लगाया जा सकता है।
एक तरफ जहां दूसरे राज्यों की सरकारें अपने-अपने यहां लोककला और लोककलाकारों को समुचित प्रोत्साहन दे रही हैं और उनका बाजार विस्तृत करने में जुटी हैं, बिहार में इसका सर्वथा अभाव दिखता है। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास योजनाएं नहीं है या नीतियां नहीं हैं। सरकार के पास फंड का भी अभाव नहीं है। सरकार घोषणाएं करती है, उत्सवों, महोत्सवों का आयोजन करवाती है, लेकिन उसका लाभ आज तक गांव देहातों में रहने वाले लोककलाकारों को नहीं मिला। कुछ कलाकार लाभ मिलने की बात करते हैं, लेकिन लाभ से उनका तात्पर्य उस मानदेय से है जो कुछेक उत्सवों में प्रस्तुतियों के बदले उन्हें प्राप्त हुआ।
चित्रकारों की स्थिति थोड़ी भिन्न है क्योंकि उन्होंने अपनी चित्रकला को समय के अनुरूप ढाल लिया और बाजारवाद के इस दौर में खुद को बचाए हुए हैं। लेकिन, पेशे से मजदूर या खेतिहर मजदूर या बंटाईदार किसान होने की वजह से गायन वादन और मंचन करने वाले कलाकारों की स्थिति ज्यादा दयनीय है। चित्रकार अगर अपनी कोई चित्र बेचता है तब उसे आमतौर पर उसका पूरा लाभ मिल जाता है, लेकिन समूह में गायन, वादन और मंचन करने वाले कलाकारों को उनका पूरा लाभ या पारितोषिक नहीं मिलता क्योंकि उसमें ठेकेदारों और बिचौलियों का भी हिस्सा होता है।
गांव देहातों से इतर शहरी इलाके में रह रहे कलाकार इसकी एक वजह राजनीति की बताते हैं। शहरी इलाकों में रह रहे ज्यादातर कलाकारों के मुताबिक, जो पिछड़ी जातियों से आते है, बिहार में सत्ता तंत्र की कमान ज्यादातर अगड़ी जातियों के हाथ में रही है जिन्होंने दलित लोककला या लोककलाकारों को बढ़ावा देने में कोई रूची नहीं दिखाई। बाद में जब सत्ता की कमान पिछड़ी जाति के नेताओं के हाथ आयी तब उन्होंने भी स्वयं को अगड़ी जाति का मान लिया। इस बात को स्वयं अगड़ी जाति के लोककलाकार भी मानते हैं। राजा सलहेस पर पुस्तक लिखने वाले अविनाश चंद्र मिश्र के मुताबिक बिहार में ज्यादातर सरकारों ने निजी मनोरंजन के लिए लोककलाकारों का इस्तेमाल किया। उनसे तमाम वादे किये लेकिन उन्हें कभी पूरा नहीं किया। ज्यादातर लोककलाकार मानते हैं कि उनके पास आजीविका के सीमित साधन होने की वजह से वो अपनी कला को विस्तार नहीं दे पाते। इसी वजह से वो अपनी कला में नए प्रयोगों का जोखिम भी नहीं उठाना चाहते और इससे लोककलाकारों के बीच यथास्थितिवाद की स्थिति पैदा हुई है, खासतौर पर गाथागायकों और नाच करने वाले कलाकारों के बीच।